


ShareThis for Joomla!
संसदीय रिवायतों का टूटना कहीं हिंसा का कारक न बन जाये
- Details
- Created on Monday, 04 February 2019 10:59
- Written by Shail Samachar

मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अन्तिम बजट आ गया है लेकिन जिस तर्ज पर यह बजट है उससे एक अब तक चली आ रही संसदीय परम्परा को बदल दिया गया। संसद की परम्परा है कि चुनावी वर्ष में सत्तारूढ़ सरकार अन्तरिम बजट में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती है। यह काम आने वाली सरकार के लिये छोड़ दिया जाता है क्योंकि जाने वाली सरकार के पास इतना समय शेष नहीं होता कि वह इन फैसलों को अमली जामा पहना सके। और आने वाली सरकारअपनी नीतियां तथा कार्यक्रम अपनी चुनावी घोषणाओं के अनुसार तय करेगी। इस परिप्रेक्ष में जाने वाली सरकार की नीतिगत घोषणाओं को चुनाव जीतने के प्रलोभनों के रूप में देखा जाता है। 2014 में लोकसभा के परिणाम 16 मई को आ गये थे। इस नाते अब भी तब तक परिणाम आ जायेंगे। इसके लिये मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग जायेगी और तब ना कोई फैंसले लिये जायेंगे और न ही लिये हुए फैसलों पर अमल हो पायेगा। इस तरह केवल एक ही फैसला अमल में आ पायेगा और वह है किसानों को छः हजार रू. की राहत पहुंचाना क्योंकि इसे दिसम्बर 2018 से लागू कर दिया गया है।
किसानों को दी गयी इस 17 रूपये प्रतिदिन की सहायता पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया रहती है यह आने वाले दिनों में सामने आ जायेगी। अभी ही देश भर के किसान दिल्ली के बाहर जमा हो गये हैं और प्रधानमन्त्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। किसानों के बाद आयकर में जो पांच लाख की छूट की बात की गयी है उसमें केवल चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे अन्य कर्मचारियों को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि कुल वेतन की आय पांच लाख से बढ़ जाती है। ऐसे कर्मचारियों को पूर्ववत ही राहत मिलेगी। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल आने वाले समय में यह सामने आयेगा कि सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिये आय सीमा आठ लाख रखी है और आयकर राहत पांच लाख। यह अपने में स्वतः विरोधी हो जाता है। इस पर आने वाले दिनों में सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौति दी जा चुकी है और अब सरकार का 5 लाख तक आयकर राहत और आरक्षण के 8 लाख की सीमा से आरक्षण पर सरकार की अपनी ही अस्पष्टता सामने आ जाती है। इसका सर्वोच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेता है यह तो आने वाले समय में ही सामने आयेगा लेकिन यह तय है कि सरकार की इस नीति पर बहस अवश्य उठेगी। इस तरह सरकार ने अन्तरिम बजट में नीतिगत फैसले करके सीधे यही इंगित किया है कि आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है।
अन्तरिम बजट में संसदीय परम्परा से हटने के साथ ही सरकार की नीयत और नीति राम मन्दिर निर्माण को लेकर भी सवालों के घेरे में आ जाती है। जब सरकार से मांग की जा रही थी कि वह इसके लिये अध्यादेश लाये तब प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अदालत के फैसले की प्रतिक्षा करेंगे। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उस जमीन के लिये आवेदन कर दिया जिसे अविवादित कहा जा रहा है। जबकि सरकार के इस अधिग्रहण को ही अदालत में ‘‘अंवाच्छित’’ कहा हुआ है। फिर सरकार तो इस प्रकरण में अदालत में पार्टी ही नही है ऐसे में अदालत सरकार के आग्रह को कैसे लेती है और कैसे इस पर त्वरित सुनवाई करती है यह देखना भी रोचक होगा। लेकिन इसी के साथ जिस ढ़ग से दो दो धर्म संसद आयोजित हुये हैं ओर 21 फरवरी को यह निर्माण शुरू कर देनें की घोषणाएं हुई हैं तथा अदालत के जजों के यहां धरने प्रदर्शन करने की चेतावनीयां दी गई हैं उससे एकदम 1992 जैसा माहौल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं बन गयी हैं। क्योंकि यह तय है कि साधु समाज का एक वर्ग इस निर्माण की शुरूआत करने आयेगा ही और निर्माण स्थल तथा उसके आसपास धारा 144 लागू ही है। ऐसे में यदि सरकार इन्हे यहां आने से रोकती नही है तब भी कानून और व्यवस्था को लेकर स्वाल उठेंगे। यदि रोकने का प्रयास करेगी तब हिंसा से इसे कोई रोक नही सकेगा। यह सब इससे होना तय लग रहा है। देश में लोकसभा चुनाव से पुर्व साम्प्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका तो अमेरिका की सीनेट में वैश्विक खतरों पर आयी डाॅन कोटस की रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले अपने हिन्दु एजैण्डा को बढ़ाने के लिये जैसे ही कदम उठायेगी उसी के साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठेगी। अमरीका की सीनेट में चर्चा में आयी इस रिपोर्ट पर भारत सरकार और भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। कोई प्रतिक्रिया न आना तथा धर्म संसद द्वारा 21 फरवरी का निर्माण कार्य शुरू करने के लिये समय तय करना इन आशंकाओं को पुख्ता करता है।
क्योंकि सरकार के पास अर्थिक मोर्चे पर भी कोई बहुत कुछ ऐसा नही है जिसे चुनावों में आसानी से भुनाया जा सके। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा पेश की गई वितिय स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का जो कर्जभार 2014 में था उसमें दिसम्बर 2018 तक 49% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ सरकार के सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नोटबन्दी के बाद देश में 1.10 करोड़ नौकरियों में कमी आयी है। यह आयोग सरकार के आंकड़ो की निगरानी और उनका आकलन करता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी 7.4% तक पहुंच गयी है। जो अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को जब जारी नही किया तब इसके अध्यक्ष पी सी मोहनन और सदस्य डा. मीनाक्षी ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। जबकि मई 2017 में नियुक्त हुए इन लोगों का कार्यकाल जून 2020 तक था। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सरकार की असफलताएं सामने है और चुनावों में इनके मुद्दा बननें की आशंका हैै। ऐसे में इन मुद्दों को चर्चा से बाहर रखने के लिये सांप्रदायिक हिंसा एक हथियार हो सकती है यह आशंका कोटस की रिपोर्ट में व्यक्त की गई है।
घातक होगी मर्यादाएं लांघती राजनीति
- Details
- Created on Monday, 28 January 2019 11:14
- Written by Shail Samachar





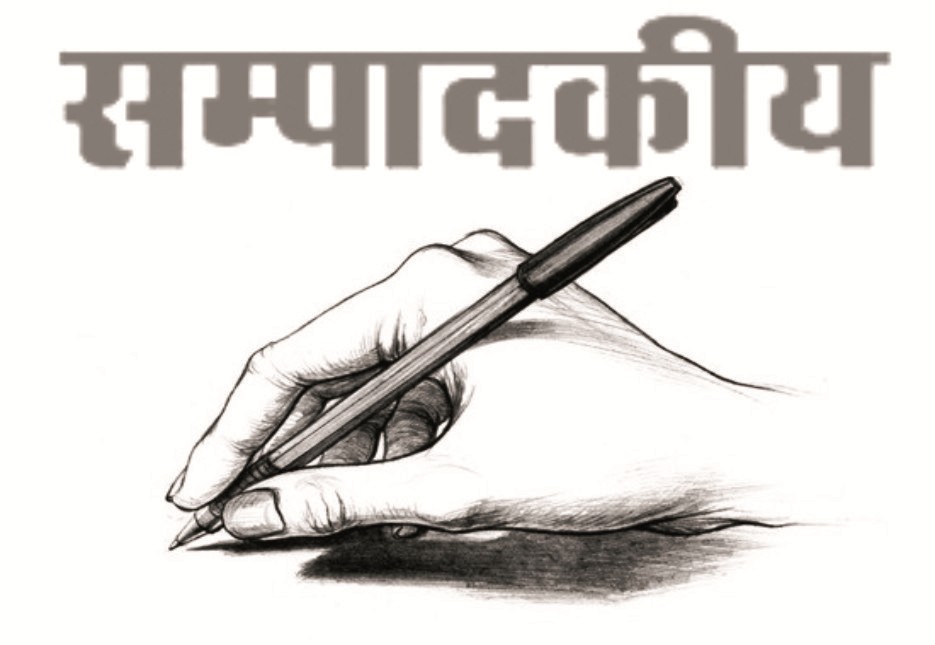
शिमला/शैल। किसी व्यक्ति या संगठन के कथ्य मे तथ्य और तर्क का अभाव होता है तब वह अपने को प्रमाणित करने के लिये ऐसी आक्रामकता का सहारा ले लेता है जिसमें भाषाई मर्यादाएं तक लांघ दी जाती है। आज देश का राजनीतिक परिदृश्य इसी दौर से गुजर रहा है। इसमें राजनीतिक दल तथ्य और तर्क के स्थान पर भाषायी अमर्यादा का शिकार होते जा रहे हैं। इस अमर्यादित भाषायी प्रयोग का अन्जाम क्या होगा? कई बार तो इसे सोचकर ही डर लगने लगता है। क्योंकि अभी एक भाजपा सांसद की जनसभा का वो वीडियो सामने आया है इसमें सांसद महोदय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी को अपने संबोधन में ‘‘पप्पु’’ कह दिया। इस संबोधन पर वहां बैठे लोगों मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सभा में से उठकर एक महिला ने सांसद महोदय से यह सवाल कर दिया कि उन्होंने राहुल गांधी को अपने संबोधन में ‘‘पप्पु’’ क्यों कहा? महिला के इस सवाल पर सारी भीड़ उत्तेजित हो गयी और पूरा वातावरण हिंसक हो चला था। इस घटना से यह सामने आता है कि जनता हर छोटी- 2 चीज पर गहरी नजर रख रही है। आज जनता को इस तरह के संबोधनों से गुमराह नही किया जा सकेगा उसे हर कथ्य के साथ तथ्य और तर्क भी देना होगा।
इस परिदृश्य में यदि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार का मोटा आंकलन भी किया जाये तो सबसे पहले यही भाषायी अमर्यादा सामने आती है जिसकी कीमत भी भाजपा को चुकानी पड़ी है। इसी कारण 2014 में प्रचण्ड बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा को दिल्ली विधानसभा के चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दिल्ली विधानसभा आने तक मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भाजपा के कुछ मन्त्रियों तक ने जिस भाषा में निशाना साधा उससे सीधे यह सन्देश गया कि यह पार्टी और इसका नियन्ता संघ किस हद तक मुस्लिम समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है। दिल्ली की प्रबुद्ध जनता में इसका सकारात्मक सन्देश नही गया और परिणास्वरूप भाजपा हार गयी। प्रधानमन्त्री मोदी ने कई बार इस तरह की ब्यानबाजी करने वाले नेताओं को जुबान पर लगाम लगाने तक की नसीहत दी जिसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ और न ही ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार और संगठन की ओर से कोई कारवाई हुई। जबकि दर्जनों वैचारिक विरोध रखने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मामले बनाए गये। सरकार के इस आचरण से भी यही सन्देश गया कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है। इसी के साथ जब आगे चलकर गो रक्षकों का अति उत्साह और लव जिहाद जैसे मामलों की स्थिति भीड़ हिंसक तक पंहुच गयी तब इससे भी इसी धारणा की पुष्टि हुई। क्योंकि इन मामलों में सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित दलित और मुस्लिम समाज ही हुआ। यह समाज अपने को एकदम असुरक्षित मानने पर विवश हुआ। इस समाज की परैवी करने के लिये मायावती और अखिलेश जैसे नेता भी सामने नही आ पाये। कांग्रेस के अन्दर राहुल ही नही बल्कि नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया में एक जिहाद ही छेड़ दिया गया। लेकिन इस सबका प्रतिफल लोस के हर उपचुनावों में भाजपा की हार के रूप में सामने आया और जब इस हार का विश्लेषण और आकलन किया गया तो इसकी पृष्ठभूमि में समाज के इस बड़े वर्ग का आक्रोश सामने आया।
संघ -भाजपा की इस वैचारिक सोच का खुलासा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के कई पाठयक्रमों में किये गये बदलाव से भी सामने आया। दीनानाथ बत्रा की कई पुस्तकों को इन पाठय्क्रमों में परोक्ष/अपरोक्ष रूप से स्थान दिया जाना इसका उदाहरण है। इस सबसे संघ- भाजपा की सामाजिक सोच और समझ को लेकर बुद्धिजीवी समाज में एक अलग ही धारणा बनती चली गयी। इस सामाजिक सोच- समझ के साथ ही प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर भी मोदी सरकार अपने को प्रमाणित नही कर पायी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की नियुक्ति 2014 के अन्ना आन्दोलन का केन्द्रिय मुद्दा था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही मनमोहन सिंह सरकार को लोकपाल विधेयक संसद में लाना और पारित करवाना पड़ा। इसके बाद आयी मोदी सरकार को केवल लोकपाल की नियुक्ति करने का ही काम बचा था जो आज तक नही हो पाया। यही नहीं मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से आपराधिक सांठ-गांठ का प्रावधान ही हटा दिया। जिसे टूजी स्कैम मनमोहन सिंह सरकार के समय केन्द्र के मन्त्री, सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी और कारपोरेशन जगत के अधिकारी जेल गये थे। उस मामले की पैरवी में मोदी सरकार के वक्त में यह सारे लोग छूट गये और अदालत को यह कहना पड़ा कि यह स्कैम हुआ ही नही था। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता का सच सामने आ जाता है। इसी सच का प्रमाण है कि सरकार राफेल मामले में संसदीय जांच का सामना करने से डर रही है। इसी कारण आज चुनावों की पूर्व संध्या पर सीबीआई को अखिलेश और हुड्डा के खिलाफ सक्रिय किया गया है। इस सक्रियता पर स्वभाविक रूप से यह प्रश्न उठ रहा है कि इन मामलों में सरकार और सीबीआई पांच वर्ष क्या करती रही। इससे अनचाहे ही सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने लगे हैं।
दूसरी ओर आर्थिक मुहाने पर भी सरकार की कोई बड़ी सकारात्मक उपलब्धि नही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करते हुए जब आठ लाख की आय तक के व्यक्ति को सरकार गरीब मान रही है तो इस मानक के आधार पर तो शायद देश की 70% से अधिक जन संख्या गरीब निकलेगी। क्योंकि देश के किसान और बागवान तो शायद 1% भी ऐसा नही निकल पायेगा जो साठ हजार रूपये प्रतिमाह कमा पा रहा हो। इस मानक से सरकार की व्यवहारिक सोच पर प्रश्न उठने लगा है। नोटबन्दी में 99% से अधिक पुराने नोट नये नोटों के साथ बदल दिये गये हैं। इकट्ठे कालेधन को लेकर किये गये सारे दावों और प्रचार का सच सामने आ गया है। इसी तरह जीएसटी में किये गये संशोधनों से यह सामने आ गया कि यह फैसला जल्दबाजी में किया गया था। इस फैसले से रोजगार के अवसर पैदा होने की बजाये काफी कम हुए हैं। इस तरह मोदी सरकार का हर बड़ा फैसला देशहित में पूरा खरा नही उतरा है। बल्कि इन फैसलों के बाद यह चुनाव सीधे-सीधे दो विचारधाराओं मे से चयन का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि देश वाम विचारधारा को देश आज तक स्वीकार नही कर सका है और दक्षिण पंथी विचारधारा की परीक्षा मोदी शासन में हो चुकी है।
क्या बेदी कमेटी की रिपोर्ट के परिदृश्य में गुजरात दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा
- Details
- Created on Monday, 21 January 2019 08:15
- Written by Shail Samachar





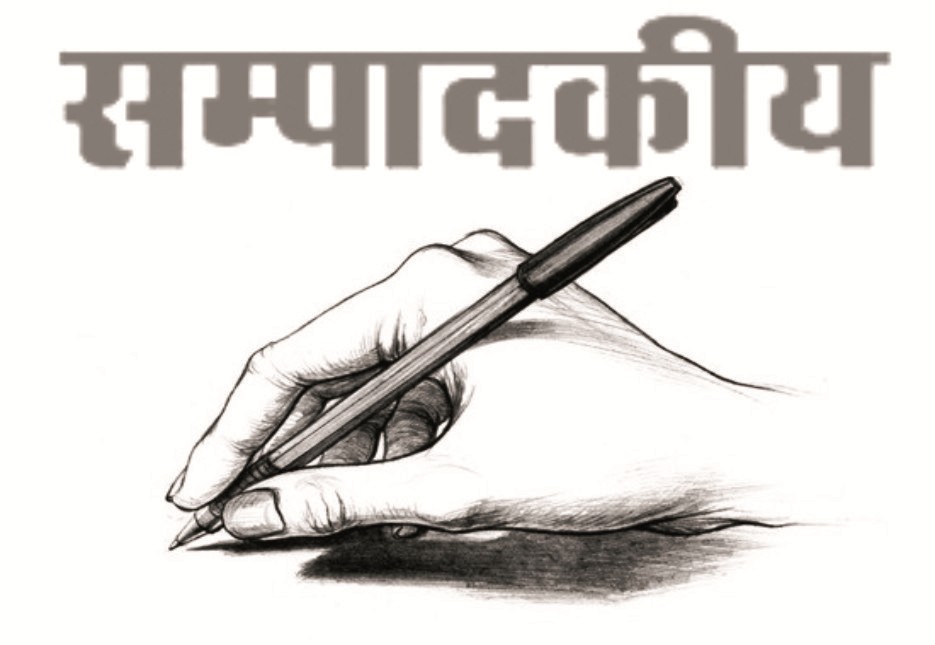
गुजरात में 2002 से 2006 के बीच जो कुछ हिंसक घटा है उसमें कितने लोगों की जान और माल की हानि हुई है इसका पूरा आंकलन शायद आज भी उपलब्ध नही है। लेकिन हिंसा को प्रोत्साहित और प्रायोजित करने के आरोप शासन /प्रशासन पर भी लगे हैं। कई राजनीतिक नेताओं पर सीधे आरोप लगे और यह आरोप आज तक पीछा नही छोड़ रहे हैं। राजनीतिक नेतृत्व इन घटनाओं के लिये इस कारण से निशाने पर आ गया था क्योंकि उस समय देश के प्रधानमन्त्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा था कि यहां पर राजधर्म का पालन नही किया गया। अब जब पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय देते हुए सज्जन कुमार जैसेे बड़े नेता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तब से एक बार फिर यह आस बंधी है कि शायद गुजरात के पीड़ितों को भी न्याय मिल पायेगा। देश ने सज्जन कुमार को सज़ा मिलने का स्वागत किया है लेकिन उसी अनुपात में जब गुजरात में एक मन्त्री को मिली ऐसी ही सज़ा के बाद उसे निर्दोष करार देकर छोड़ देने पर अफसोस भी जाहिर किया है।
गुुजरात में जो कुछ घटा है उसमें एक आरोप वहां पर फर्जी एनकाऊंटर दिखाये जाने का भी पुलिस प्रशासन पर लगा है। इन फर्जी मुठभेड़ों पर सर्वोच्च न्यायालय में 2007 में वीजी वर्गीज और जावेद अख्तर तथा शबनम हाशमी ने दो याचिकाएं दायर की थी। इनमें सत्रह मामले फर्जी एनकाऊंटर के आरोपों के उठाये गये थे। यह याचिकाएं 2007 में दायर हुई थी और इनके दायर होने के बाद गुजरात सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए इनकी जांच के लिये स्पैशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इस एसटीएफ का मुखिया पुलिस अधिकारी ए. के. शर्मा को लगाया गया। लेकिन ए. के. शर्मा की नियुक्ति पर शबनम हाशमी ने कुछ एतराज उठाये। एतराज में ए.के. शर्मा और नरेन्द्र मोदी के बीच घनिष्ठ संबंध होने का भी गंभीर आरोप था। जब यह सबकुछ सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तब शीर्ष अदालत ने इसकी माॅनिटरिंग के लिये एक कमेटी का गठन कर दिया। इसका चेयरमैन शीर्ष अदालत के ही पूर्व जज एम वी शाह को बनाया गया लेकिन जस्टिस शाह ने इस जिम्मेदारी को स्वीकारने में असमर्थता दिखाई। जस्टिस शाह के असमर्थता दिखाने के बाद गुजरात सरकार ने अपने ही स्तर पर इस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश के आर ब्यास को नियुक्त कर दिया जबकि जस्टिस शाह की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी। जब जस्टिस ब्यास की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आयी तब शीर्ष अदालत ने यह जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व जज जस्टिस एचएस वेदी को सौंप दी।
जस्टिस शाह की नियुक्ति 25 जनवरी 2012 को हुई थी और उनके स्थान पर जस्टिस बेदी की नियुक्ति 12 मार्च 2012 को हुई। जब यह माॅनिटरिंग बनाई गयी थी तब इसकी नियुक्ति में यह कहा गया था कि वह इस नियुक्ति के तीन माह के भीतर पूर्ण या अन्तरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। इस कमेटी के सामने जो सत्रह मामले आये थे उनकी जांच के लिये पूरी प्रक्रिया अपनाई गयी। इस तरह बेदी कमेटी की जो फाईनल रिपोर्ट तैयार हुई उसे सार्वजनिक नही किया गया। गुजरात सरकार इसके सार्वजनिक किये जाने का विरोध कर रही थी। यह विरोध इस हद तक गया कि जिन याचिकाओं के बाद एसटीएफ का गठन हुआ और उसकी माॅनिटरिंग के लिये शीर्ष अदालत को कमेटी बनानी पड़ी उन याचिकाकर्ताओं को भी इस कमेटी की रिपोर्ट नही दी गयी। यह रिपोर्ट न दिये जाने पर फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया और शीर्ष अदालत ने 18 दिसम्बर 2018 को यह याचिकाकर्ताओं को दिये जाने के आदेश किये। शीर्ष अदालत के इन आदेशों की अनुपालना में जस्टिस बेदी ने 20 दिसम्बर 2018 को यह 220 पन्नो की रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस बेदी की रिपोर्ट में इस कमेटी के सामने आये सत्रह मामलों में से तीन मामलों को पुलिस हिरासत में हुई मौत करार देते हुए इनमें गंभीर कारवाई किये जाने की संस्तुति की है। जब जस्टिस बेदी कमेटी इन मामलों को देख रही थी उसी दौरान इन दंगो को लेकर एक पत्रकार राणा अयूब ने एक स्टिंग आपरेशन किया है। यह स्टिंग आपरेशन गुजरात फाईल्ज़ पुस्तक के रूप में सामने आ चुका है। इस आपरेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे दर्ज है और इस स्टिंग आप्रेशन का जिक्र जस्टिस बेदी की रिपोर्ट में भी आया है। इस तरह जस्टिस बेदी की रिपोर्ट और राणा अयूब की गुजरात फाईल्ज़ के परिदृश्य में गुजरात दंगो को लेकर जो कुछ सामने आया है उसके परिदृश्य में इस पर नये सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता आ खड़ी होती है।
जस्टिस बेदी ने अपनी रिपोर्ट में इन मामलों को लेकर जो कुछ कहा है वह उन्ही के शब्दों में पाठकों के सामने रख रहा हूं ताकि इस पर आप अपने स्तर पर राय बना सके।
I have, therefore, taken a conscious decision that initially action will be sussested asainst only those police officers whose participation was admitted or prima facie proved leaving it open for others who are subsequently found to have been involved in conspiracy or in any other manner in regular court proceedings, to be arraigned later as per law. thease directions must be read into the three matters in which I have found prima facie evidence of custodial killings.
आर्थिक आरक्षण पर उठते सवाल
- Details
- Created on Tuesday, 15 January 2019 05:44
- Written by Shail Samachar





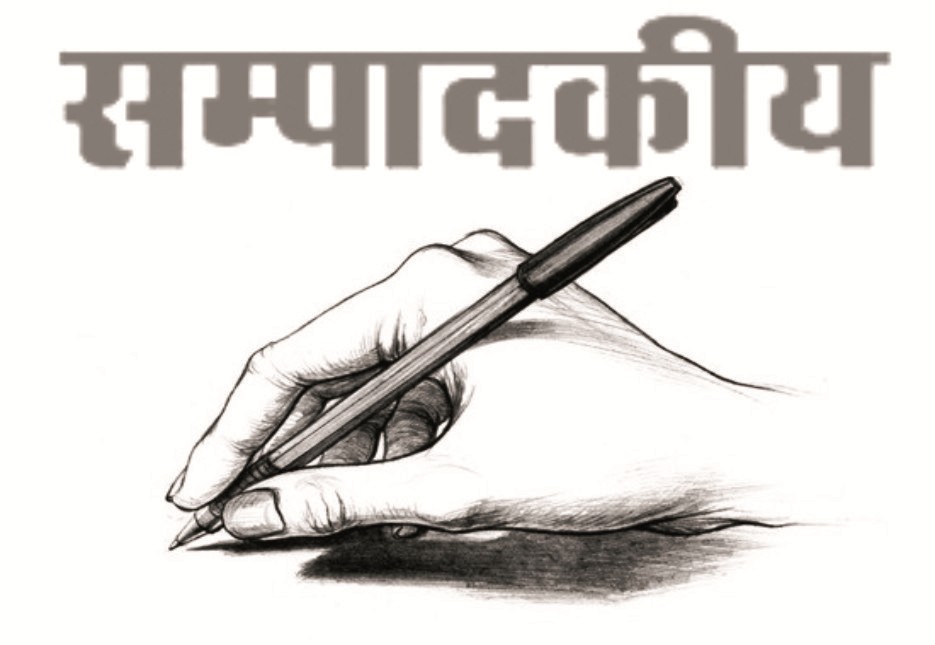
आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान करने के लिये संविधान में संशोधन किया गया है। यह आर्थिक रूप से गरीब अगड़े कौन होंगे इसके लिये ऐसे लोगों के परिवार की आय सीमा आठ लाख तय की गयी है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक ज़मीन नही होनी चाहिये। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिये मकान के एरिया का मानक साथ रखा गया है। इस तरह मोटे तौर पर आठ लाख की आय तक व्यक्ति को गरीब माना गया है। इस तरह गरीब की पहचान उसके बीपीएल परिवार होने के रूप में की जाती है। गरीबी के इन मानकों से स्पष्ट हो जाता है कि इस आरक्षण का लाभ लेने के लिये व्यक्ति का बीपीएल होना जरूरी होगा। आठ लाख तक की आय का प्रमाणपत्र लाभार्थि के पास होना आवश्यक होगा। सवर्ण होने का जाति प्रमाणपत्र भी साथ रखना आवश्यक होगा। इस समय 2.5 लाख तक की आय वाले को आयकर से छूट हासिल है लेकिन अब जब गरीब होने के लिये आठ लाख की आय सीमा रख दी गयी है तो स्वभाविक है कि इस आय तक का हर व्यक्ति आयकर से छूट चोहगा। क्या सरकार आठ लाख तक की आय पर आयकर से छूट दे पायेगी यह पता तो आने वाले समय में ही लगेगा लेकिन यह तय है कि इसके लिये मांग उठेगी और या तो उसे मानना पड़ेगा। फिर आठ लाख के मानक में संशोधन करना प़डेगा। केन्द्र सरकार ने यह मानक अपनी सेवाओं के लिये तय किये हैं और राज्य सरकारों को इनमें फेरबदल करने की छूट दे रखी है। ऐसे में बहुत संभव है कि हर राज्य में इन मानकों में भिन्नता आ जाये क्योंकि हर जगह जमीन की कीमतों में अन्तर होगा ही। इसलिये इन मानकों में आने वाले संभावित अन्तः विरोधों के चलते इस आरक्षण को अमली जामा पहनाना इतना आसान नही होगा।
देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसमें सामाजिक रूप से पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिये एक माध्यम आरक्षण का भी सुझाया गया है। लेकिन यह आरक्षण का प्रावधान संविधान के लागू होने के साथ ही शुरू नही हो गया था। बल्कि 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद इन सामाजिक तौर पर पिछड़ो की पहचान के लिये काका कालेश्वर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर लम्बे विचार विमर्श के बाद इन पिछडों की पहचान अनुसूचित जातियों और जन जातियों के रूप में की गयी थी और फिर इनके लिये सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था जो आजतक चल रहा है। इसके बाद 1979 में फिर अन्य पिछड़ा वर्गाें की स्थिति पर संसद में चर्चा उठी और इनकी पहचान के लिये वीपी मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट 1980 में आयी और इस कमेटी की सिफारिशों पर 1990 में वीपी सिंह की सरकार के वक्त फैसला हुआ तथा इन पिछड़ा वर्गों के लिये भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मण्डल की सिफारिशों पर अमल करने से पहले इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों को अपने सुझावों के लिये भेजा गया था। कई राज्यों ने इस पर अपनी राय भेजी थी और कुछ ने नहीं। हिमाचल में उस समय शान्ता कुमार की सरकार थी लेकिन इस सरकार ने अपनी कोई राय नही भेजी थी।
इसी के साथ यदि इस विधयेक के उद्येश्यों पर नजर डाली जाये तो उसमें यह कहा गया है कि यह लाभ उन वर्गों को मिलेगा जिन वर्गों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नही है। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसमे निश्चित रूप से यह आंकड़ा जुटाना होगा कि इस समय देश में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी नौकरियां सरकार में हैं। इनमे से कितनी किस वर्ग से भरी हुई है अभी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रखे गये आरक्षित कोटे के मुताबिक व्यवहारिक रूप से इन्हें नौकरियां मिल पायी हैं या नही। यदि इन्हे ही पूरा कोटा नही मिल पाया है तो फिर पहली मांग इनका कोटा पूरा करने की आयेगी। इस स्थिति का दूसरा अर्थ यह होगा कि सवर्ण जातियों को सरकार नौकरियों में पहले ही पूरा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इस आधार पर इन गरीब सवर्णों को अभी सरकारी नौकरियों में वांच्छित आरक्षण मिलने में समय लगेगा। हां शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जायेगी लेकिन इस सबके लिये आंकड़े जुटाने और उनका आकंलन करने में समय लगेगा। इस आंकलन पर भी सहमति बनानी होगी। कायदे से यह सबकुछ इस विधेयक को लाने से पहले हो जाना चाहिये था। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह सबकुछ राजनीतिक जल्दाबाजी में किया गया है।
इस आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आ चुकी है। गुजरात सरकार ने 2016 में इसी दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिये अध्यादेश जारी किया था जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार इसकी अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गयी हुई है और उसकी अपील अभी तक लंबित पड़ी हुई है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने को सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की पीठ इन्दिरा साहनी मामले में पहले ही निरस्त कर चुकी है। कई उच्च न्यायालय भी कई राज्यों में लाये गये ऐसे प्रावधान को रद्द कर चुके हैं। इसलिये अब किये गये प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय की सहमति मिल पाती है या नही इसका पता तो आने वाले दिनों मे ही लगेगा। लेकिन यह विधयेक लाकर मोदी सरकार जो लाभ लेना चाहती थी उसमें कांग्रेस ने इसे राज्य सभा में समर्थन देकर सफल रूप से सेंध लगा दी है क्योंकि यदि राज्य सभा में कांग्रेस समर्थन न देती है तो यह पारित नहीं हो पाता। अभी कई दलित संगठन इसके विरोध में उतरने लग पड़े हैं उन्हें लग रहा है कि इसके माध्यम से आने वाले दिनों में उनके कोटे पर डाका डाला जायेगा। इस परिदृश्य में यह संभावना बहुत बलवती लग रही है कि यह विधेयक लाकर सरकार को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। क्योंकि दलित नाराज हो रहे हैं और सवर्णों में कांग्रेस पूरी बराबर की भागीदार बन गयी है।
क्या राम मन्दिर पर 1992 दोहराया जायेगा
- Details
- Created on Wednesday, 09 January 2019 11:02
- Written by Shail Samachar





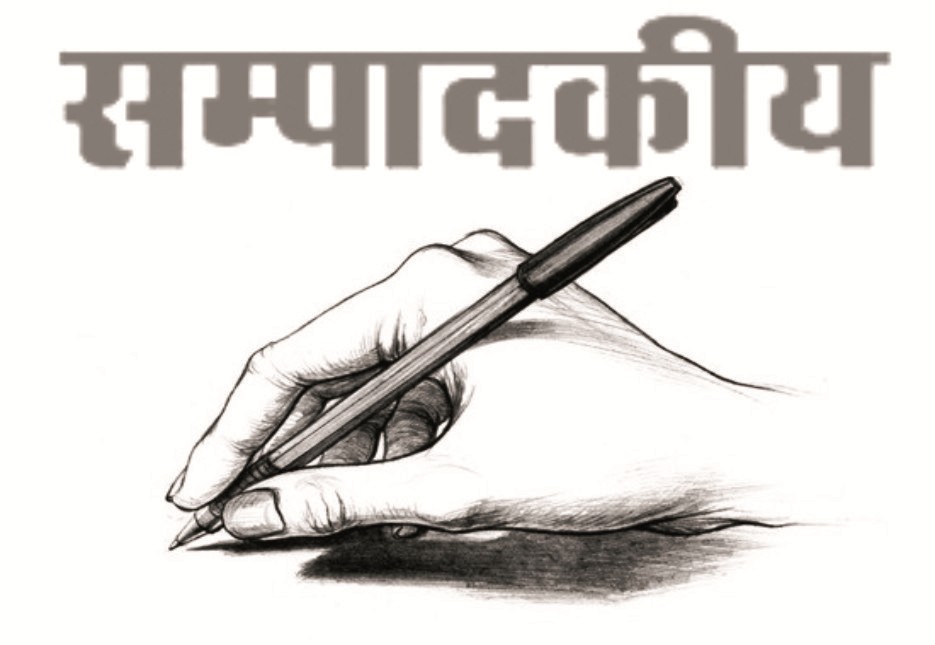
राम मन्दिर मुद्दे की सर्वोच्च न्यायालय ने दैनिक आधार पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह इन्कार उस समय आया है जब देश के कानून मन्त्री रविशंकर प्रसाद ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई फास्टट्रैक करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने टीवी साक्षात्कार में कहा है कि सरकार इस मामले में अदालत के फैसले का इन्तजार करेगी और इसमें अध्यादेश लाने का विकल्प नही चुनेगी। भाजपा/ संघ के लिये राम मन्दिर निर्माण एक लम्बे अरसे से केन्द्रिय मुद्दा चला आ रहा है। दिसम्बर 1992 में इसी प्रकरण पर भाजपा की चार राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन की भेंट चढ़ गयी थी। 1992 के बाद केन्द्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। दो बार स्व. वाजपेयी के नेतृत्व में गठबन्धन की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जो प्रचण्ड बहुमत मिला है ऐसा शायद दूसरी बार नही मिले। इस बार भाजपा किसी सहयोगी पर निर्भर नही है। 2014 में यह वायदा भी किया गया था कि राममन्दिर का निर्माण उसकी पहली प्राथमिकता होगी। बल्कि आजतक संघ/ जनसंघ भाजपा के जो भी हिन्दुवादी मुद्दे रहे हैं उन्हे अमली जामा पहनाने का इस बार ऐसा अवसर मिला था जो निश्चित रूप से फिर नही मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था भले ही वह राज्य सभा में लटक जाता लेकिन इससे भाजपा की नीयत पर किसी को भी सन्देह करने का अवसर न मिलता उल्टेे विरोधी जनता के सामने जबावदेही की भूमिका में आ जाते। लेकिन इस पूरे शासनकाल में मोदी सरकार ने एक भी दिन ऐसा कोई कदम नही उठाया। इससे संघ/भाजपा की नीयत पर जो सवाल/सन्देह उभरे हैं उनका वर्तमान में कोई जबाव नही है।
राम मन्दिर के मुद्दे पर संघ विश्व हिन्दु परिषद, साधु समाज और कई भाजपा/सांसदो/मन्त्रियों के जो ब्यान आये हैं और आ रहे हैं वह एकदम प्रधानमन्त्री के स्टैण्ड से अलग हैं। यह सभी लोग लोकसभा चुनाव से पहले मन्दिर के निर्माण की बातें कर रहे हैं। सरकार पर इस संद्धर्भ में कानून लाने की बात की जा रही है। इसके लिये केवल अध्यादेश लाने का ही विकल्प बचा है क्योंकि सामान्य विधेयक लाकर उसे कानून बनवा पाने की अब वक्त नही बचा है और सरकार अच्छी तरह जानती है। इस परिदृश्य में प्रधानमन्त्री का अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करना 1992 दोहराये जाने का स्पष्ट संकेत बन रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है यह सही में प्रधानमन्त्री और इन अन्यों के बीच गंभीर मतभेद चल रहे हैं क्योंकि अब तक जो कुछ सरकार बनने के बाद घटा है वह इसी ओर संकेत करता है कि यह सब कुछ रणनीतिक है। क्योंकि जब भी संघ/भाजपा और मोदी के कुछ मन्त्रीयों के विवादित के ब्यान आते थे तब प्रधानमन्त्री रस्मी नाराजगी और चुप रहने की नसीहत का ब्यान देते रहे जिसका व्यवहार में कोई अर्थ नही रहा। देश जानता है कि मण्डल के विरोध में उठा आरक्षण विरोधी आन्दोलन कितना उग्र हो गया था। उसमें आत्मदाह तक हुए। वी पी सिंह सरकार गिरने के साथ ही यह आन्दोलन बन्द तो हो गया लेकिन आरक्षण के खिलाफ भावना और धारणा बनी रही। अब जब मोदी सरकार आयी तब फिर कई राज्यों से आरक्षण को लेकर आवाजें उठी। मांग की गयी कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका बन्द करो। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा और शीर्ष अदालत ने फैलसा दे दिया लेकिन मोदी सरकार ने संसद का सहारा लेकर यह फैसला बदल दिया। इससे भाजपा सरकार और संघ की नीयत और नीति पर सवाल उठे हैं यही आचरण धारा 370 को लेकर सामने आया हैं इस तरह ऐसे कई मुद्दे हैं जहां संघ/भाजपा की कथनी और करनी का फर्क खुलकर सामने आ गया है।
इस परिदृश्य में आज राम मन्दिर को लेकर यह सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय से आज जो इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई करने की मांग की जा रही है क्या यह मांग और प्रयास 2014 में मोदी सरकार बनने के साथ ही नही हो जाना चाहिये था? लेकिन उस समय ऐसा नही किया गया क्योंकि उस समय कोई चुनाव नही होने जा रहे थे। आज चुनावों की पूर्व संध्या पर राम मन्दिर को लेकर जो वातावरण समाज में खड़ा किया जा रहा है उसके परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बातायेगा। लेकिन जो कुछ भी घटता नज़र आ रहा है वह शायद देशहित में नही होगा। लगता है राम मन्दिर को लेकर 1992 को दोहराने की नीयत और नीति अपनाई जा रही है।



