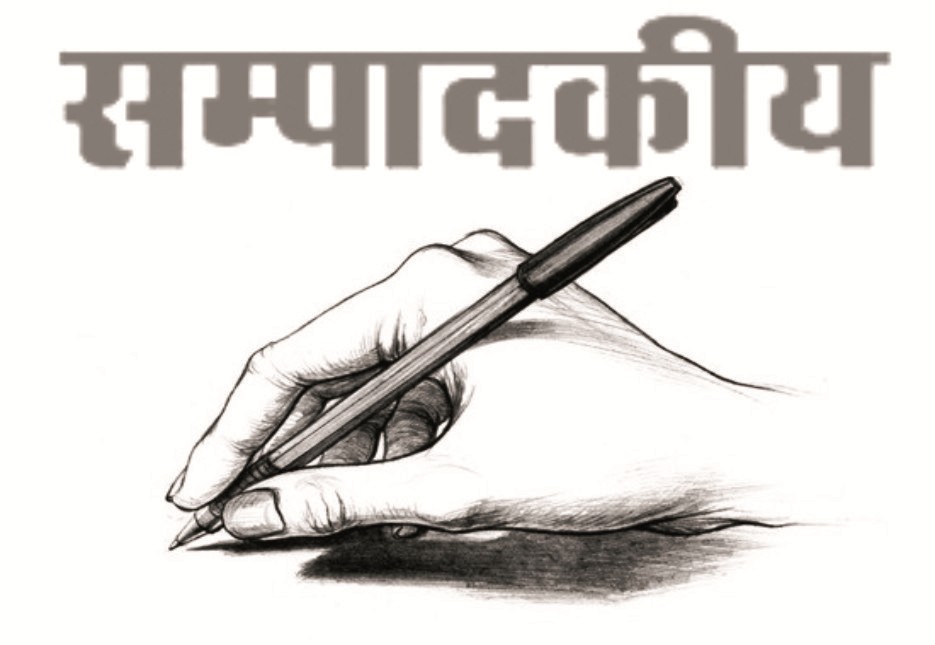ShareThis for Joomla!
रोजी-रोटी का संकट होगा तालाबन्दी का अन्तिम परिणाम
- Details
- Created on Sunday, 12 April 2020 03:25
- Written by Shail Samachar
 कोरोना का कहर कितना भयानक हो उठा है इसका अन्दजा इसी से लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार को एक अध्यादेश लाकर प्रधानमंत्री से लेकर सांसदो तक के वेतन भत्तों और पैन्शन पर एक वर्ष के लिये 30% की कटौती घोषित करनी पड़ी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से अपने ऊपर यह 30% की कटौती आयत कर ली हैं प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से लेकर विधायकों तक ने यह कटौती अपने ऊपर से पहले ही महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आन्धप्रदेश की सरकारों ने तो अपने कर्मचारियों तक के वेतन में 75% से लेकर 50% तक कटौती घोषित कर दी है। केन्द्र सरकार ने तो सांसद निधि भी दो वर्ष के लिये निरस्त कर ली। सांसदों की ऐच्छिक निधि पर भी कर लगा दिया है। हिमाचल जैसे कुछ राज्यों ने भी विधायक क्षेत्र विकास निधि पर दो वर्ष के लिये रोक लगा दी हैं। इन सारे कदमों का तर्क कोविड-19 की रोकथाम के लिये धन जुटाना कहा गया है। संभव हे कि हर राज्य सरकार को यही कदम उठाने पड़े और अन्त में इस सबका परिणाम वित्तिय आपतकाल की घोषणा के रूप में सामने।
कोरोना का कहर कितना भयानक हो उठा है इसका अन्दजा इसी से लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार को एक अध्यादेश लाकर प्रधानमंत्री से लेकर सांसदो तक के वेतन भत्तों और पैन्शन पर एक वर्ष के लिये 30% की कटौती घोषित करनी पड़ी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से अपने ऊपर यह 30% की कटौती आयत कर ली हैं प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से लेकर विधायकों तक ने यह कटौती अपने ऊपर से पहले ही महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आन्धप्रदेश की सरकारों ने तो अपने कर्मचारियों तक के वेतन में 75% से लेकर 50% तक कटौती घोषित कर दी है। केन्द्र सरकार ने तो सांसद निधि भी दो वर्ष के लिये निरस्त कर ली। सांसदों की ऐच्छिक निधि पर भी कर लगा दिया है। हिमाचल जैसे कुछ राज्यों ने भी विधायक क्षेत्र विकास निधि पर दो वर्ष के लिये रोक लगा दी हैं। इन सारे कदमों का तर्क कोविड-19 की रोकथाम के लिये धन जुटाना कहा गया है। संभव हे कि हर राज्य सरकार को यही कदम उठाने पड़े और अन्त में इस सबका परिणाम वित्तिय आपतकाल की घोषणा के रूप में सामने।इस तरह के कई वित्तिय फैसले रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्रीयों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने यह चुनौती आनी ही थी जिसका संकेत बैंकों के फेल होने से मिलना शुरू हो गया था। आज कोरोना के कारण जब हर व्यक्ति अपने में डर गया है तो परिणाम पूर्ण तालाबन्दी और कफ्रर्यू के रूप में सामने आ गया है। एक झटके में सारी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है। स्थिति इतनी विकट हो गयी है कि गतिविधियां पुनः कब चालू हो पायेंगी यह कहना कठिन हो गया है। यह स्पष्ट नही है कि उद्योगों को पुनः उत्पादन में आने में कितना समय लग जोयगा। इन उद्योगों पर जितना बैंकों के माध्यम से निवेश हुआ पड़ा है वह कितना सुरिक्षत बच पायेगा यह कहना आसान नही है। शायद इसी सबके सामने रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में वित्तिय अपातकाल लागू किये जाने के आग्रह की याचिकाएं आ चुकी हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए याचिकाएं आ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग भी एक याचिका के माध्यम से आ चुकी है। यदि आर्थिक उत्पादन की गतिविधियां और ज्यादा देर तक बन्द रही तो एक बड़े वर्ग के लिये रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आईएलओ के अध्ययन के मुताबिक देश में चालीस करोड़ लोगों को रोज़गार पर गंभीर संकट खड़ा हो जायेगा। लेकिन जहां देश इस तरह के संकट से गुजर रहा है वहीं पर एक वर्ग कोरोना के फैलाव के लिये तब्लीगी समाज को जिम्मेदार ठहराने के प्रयासों में लगा हुआ है। यह वर्ग इस तथ्य को नजरअन्दाज कर रहा है कि रामनवमी के अवसर पर कई जगह हिन्दु समाज ने भी तालाबन्दी को अंगूठा दिखाते हुए आयोजन किये हैं रथ यात्राएं तक निकाली गयी हैं। इस आश्य के दर्जनों वीडियोज़ सामने आ चुके है जिनका खण्डन करना कठिन है। ऐसे में एक ही जिम्मेदार ठहराने के प्रयासों में लगे हुए लोग न तो सरकार के ही शुभचिन्तक कहे जा सकते हैं और न ही समाज के। क्योंकि जब बिमारी के डर के साथ ही भूख का डर समान्तर खड़ा हो जायेगा तब उसका परिणाम केवल क्रान्ति ही होता है।
ताली थाली के बाद दीपक पर उम्मीद
- Details
- Created on Sunday, 05 April 2020 17:40
- Written by Shail Samachar



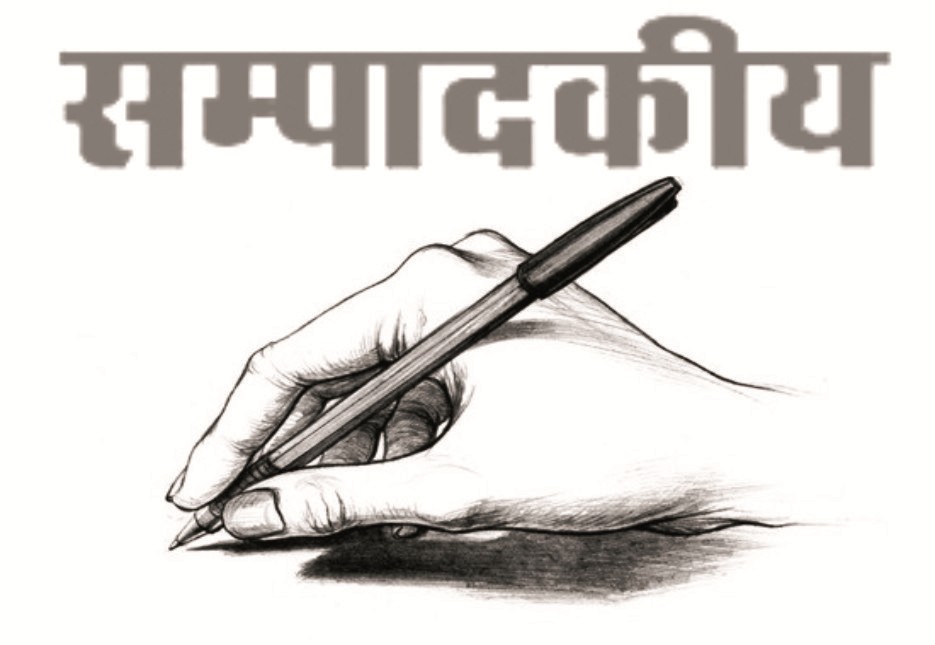
प्रधानमंत्री का आह्वान है इसलिये यह पूरा किया ही जायेगा क्योंकि इस समय सारी उम्मीदें उन्ही पर ही टिकी हुई हैं। इसलिये आज सवाल भी प्रधानमंत्री से ही किया जायेगा। अभी तालाबन्दी के दस दिन शेष हैं। पहले दस दिनों में ही राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे पाने में अपनी असर्मथता जताई है। वेतन में 75%,60%,50% और दस प्रतिशत की कटौती अगले आदेशों तक की गयी है। पैन्शन में भी दस प्रतिशत की कटौती की गयी है। हिमाचल जैसे राज्य ने नये वर्ष के पहले ही सप्ताहमें कर्ज लेकर शुरूआत की है। आरबीआई ने हर तरह के जमा पर ब्याज दरें कम की हैं। इसमें छोटी बचतें और चालू एफडी भी शामिल है। इसका तर्क यह दिया गया है कि तालाबन्दी के कारण राजस्व के संग्रहण में कमी आयी है। लेकिन तालाबन्दी तो पिछले वित्तिय वर्ष के अन्तिम सप्ताह मे लागू की गयी थी। 24 मार्च तक तो कोई तालाबन्दी नही थी सारा काम यथास्थिति चल रहा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सप्ताह में सरकारों की हालत यह हो गयी कि वह पूरा वेतन दे पाने में असमर्थ हो गयी। तालाबन्दी के कारण देश के चालीस करोड़ से अधिक के लोग प्रभावित हुए हैं जिन्हे यह पता नही है कि उन्हे फिर से रोज़गार कब मिल पायेगा। देश की आज़ादी के समय तो करीब डेढ़ करोड लोगों ने ही पलायन किया गया था। सोलह अगस्त 1947 को 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गये थे और 72 लाख ही पाकिस्तान से भारत आये थे। लेकिन उस पलायन का दर्द यह लोग आज भी महसूस करते हैं। परन्तु आज तो अपने देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर प्रतिबन्ध है। बलिक राज्यों के अपने भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। सीमाएं सील कर दी गयी हैं और सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में लोग बेघर होकर बैठे हैं। आज जब प्रधानमंत्री ने देश से दीपक जलाकर रोशनी करने का आह्वान किया है तब यदि इन लोगों के लिये भी कोई स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है तो शायद इन्हे कुछ साहस मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।
यही नही जिस महामारी के कारण आज ये हालात पैदा हुए हैं उससे बचने के लिये कोई दवाई तो अभी तक नही बन पायी है परन्तु जो सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक हैं उनकी भी आपूर्ति नही हो पा रही है। जो डाक्टर मरीजों के उपचार में लगे हुए हैं उन्हे ही यह सुरक्षा उपकरण पूरी मात्रा में उपलब्ध नही हैं। उपचार में लगे डाक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की हर राज्य से कमी की शिकायतें आ रही है। ऐसे में कई जगहों पर डाक्टरों नर्सो ने त्यागपत्र तक देने का प्रयास किया है। इस आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिये समय रहते उचित कदम नही उठाये गये हैं यह पूरी तरह सामने आ चुका है। बल्कि तालाबन्दी के बाद भी जिस तरह से सर्विया आदि देशों को इस आवश्यक सामान का निर्यात किया गया है उससे सरकारी प्रबन्धों और संवदेना पर गंभीर सवाल उठ खडे़ हुए हैं । इस वस्तुस्थिति में भी निज़ामुद्दीन प्रकरण को जिस तरह से कुछ हल्कों में हिन्दु-मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। वह सामाजिक सौहार्द की दिशा में बहुत घातक सिद्ध होगा यह तय है। क्योंकि यह प्रकरण भी शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। इसमें दर्ज हुए मामले अदालत तक पहुंचेगे ही। तब यह सवाल उठेगा ही कि देश की गुप्तचर ऐजैन्सीयां क्या कर रही थी। उनकी सूचनाएं क्या थी और उन पर केन्द्र और दिल्ली सरकार ने क्या किया। मरकज़ के साथ लगते पुलिस थाने ने क्या भूमिका अदा की। यह सवाल एक बार चर्चा में आयेंगे ही। ऐसे में आज यदि प्रधानमंत्री इन सारे आसन्न सवालों पर देश को संबोधित कर जाते तो शायद कोरोना का हिन्दु-मुस्लिम होना रूक जाता। अब देखना दिलचस्प होगा की दीपक के प्रकाश में यह महामारी हिन्दु-मुस्लिम होने से बच पाती है या नही।
कर्फ्यू और तालाबन्दी भय का कारण बन रहे हैं
- Details
- Created on Friday, 27 March 2020 13:38
- Written by Baldev Shrama



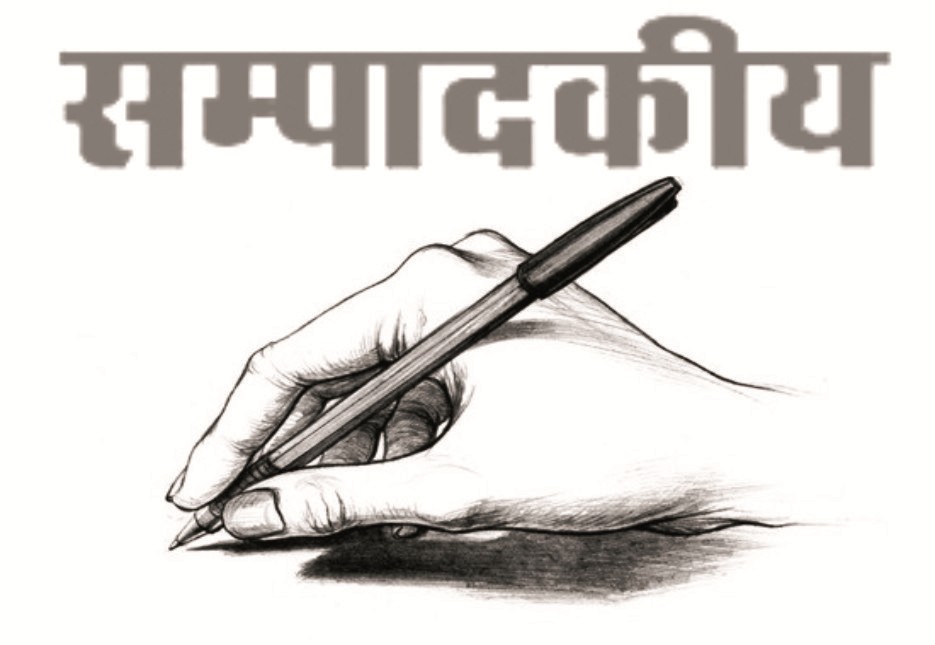
इस तरह जो कुछ यह घटा है उससे कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुये है। पहला सवाल तो यही है कि न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकारों ने जनता को इस संबंध में तैयार होने का समय दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्या जो स्थिति सामने दिख रही है वास्तव में उससे भिन्न है ? दूसरा सवाल है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी के शुरू में ही पी पी ई उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने की एडवाईजरी जारी कर दी थी तो फिर केन्द्र 19 मार्च तक इसका निर्यात क्यों करता रहा। आज हर अस्पताल पी पी ई उपकरणों की कमी से जूझ रहा है। इसका कोई भी जबाव सामने नही आया है। तीसरा बड़ा सवाल है कि जब देश भर में सामाजिक आयोजनों पर सोशल डिसटैन्सिग के मकसद से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तो शिवराज सिंह चैहान और योगी आदित्यनाथ के आयोजन कैसे हो गये क्या यह लोग प्रधानमंत्री के आदेशों की भी परवाह नही करते हैं? क्योंकि इन आयोजनों से अनचाहे ही यह सन्देश गया है कि स्थिति उस तरह की गंभीर नही है जैसी की सरकार के कदमों से लक्षित हो रही है। बल्कि यह संदेश जा रहा है कि सरकार जानबूझकर जनता का डरा रही है।
स्मरणीय है कि धारा 144 का ही विस्तारित रूप है कर्फ्यू और तालाबन्दी/प्रशासन सामान्यत यह कदम कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उठाता है। जब किसी कारण से जनाक्रोष उग्र हो उठता है और उससे जानमाल को क्षति पहुंचने की आशंका बन जाती है तब प्रशासन इन कदमों के सहारे स्थिति पर नियन्त्रण बनाये रखने का प्रयास करता है। उसमें भी जनता को पूर्व चेतावनी दी जाती है। इस समय जिस तरह से एकदम बिना कोई समय दिये कर्फ्यू और तालाबन्दी लागू कर दिये गये उससे तो एकदम आघोषित आपातकाल की स्थिति बना दी गई है। जबकि जनता तो इस महामारी से अपने आप ही डरी हुई है क्यांेकि अभी तक इसकी कोई दवाई तक उपलब्ध नही है। ऐसे में जब सरकार के आदेशों से पूरे देश की हर गतिविधि थम गई है तो उसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर किस तरह का पडेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। छोटा बड़ा सारा उद्योग धन्घा बन्द हो गया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। सरकार ने इन लोगों की सहायता के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे व्यवहार में उतारने के लिये कितना समय लगेगा जबकि यातायात के सारे साधन सरकारी आदेशों से बन्द हो चुके हैं। खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कितना मानवश्रम चाहिये। जब यह मानव संसाधन व्यवहारिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगेगा तो क्या उससे सोशल डिस्टैनसिंग प्रभावित नही होगी। क्या तालाबन्दी और कर्फ्यू लगाने से पहले यह विचार किया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जायेगी। अभी तीन दिन के कर्फ्यू में ही यह हालात को गये है कि लोगों को राशन की दूकानों से खाली हाथ लौटना पडा है। फिर यह तय नही है कि सोशल डिसटैन्सिग को कितने समय तक जारी रखना पडेगा। इस समय सरकार के ये कदम जनता में जन विश्वास की बजाये डर का कारण बनते जा रहे है और यही सबसे घातक है।
जनता कर्फ्यू से आगे क्या होगा
- Details
- Created on Sunday, 22 March 2020 14:23
- Written by Shail Samachar
देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है और यह संकट कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अन्ततः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से आह्वान करना पड़ा है कि रविवार को पूरा देश सुबह सात बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पूरी ईमानादारी से पालन किया जाना चाहिये। क्योंकि जो बीमारी संक्रमण से फैलती हैं उसमें संक्रमण को कम करने के लिये एक दूसरे से मिलना ही बन्द करना पड़ता है और यह काम कर्फ्यू से ही किया जा सकता है। कोरोना का अभी तक कोई अधिकारिक ईलाज सामने नही आया है ऐसे में सावधानी ही पहला कदम रह जाता है। प्रधानमंत्री ने जो कर्फ्यू का आह्वान किया है उससे निश्चित रूप से संक्रमण की संभावना काफी कम हो जायेगी क्योंकि ‘‘ जान है तो जहान है’’ को मानते हुए हर आदमी इसका पालन भी करेगा। बल्कि यदि आवश्यकता हो तो कुछ दिनों बाद यह प्रयोग फिर से कर लिया जाना चाहिये।
कोरोना को दस्तक दिये हुए काफी समय हो गया हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किये हुए एडवाईज़री तक जारी की है। भारत में भी केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री के आह्वान से पहले ही कई कदम इस दिशा में उठा रखे हैं। इन्ही कदमों के चलते शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा घर आदि पूरे देश में बन्द किये जा चुके है। सामाजिक समारोहों और सांस्कृतिक समारोहों के लिये भी एडवाईज़री जारी हो चुकी है। मन्दिरों के कपाट बन्द कर दिये गये हैं। जिस भी गतिविधि से संक्रमण की संभावना बनती है उसी को बन्द किया जा चुका है। स्वभाविक है कि जिस बीमारी को कोई ईलाज सामने न हो उसमें परहेज़ ही सबसे पहला कदम रह जाता हैं इसलिये प्रधानमंत्री का कर्फ्यू का आह्वान एक स्वागत कदम है जिसका पूरा समर्थन किया जाना चाहिये।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि सरकार कोविड-19 के नाम से आर्थिक मोर्चे पर वित्तमन्त्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन करने जा रही है। यह टास्क फोर्स आने वाले दिनों में कुछ आर्थिक फैसले लेगी। प्रधानमंत्री ने इन फैसलों का कोई सीधा संकेत नही दिया है। लेकिन इन संभावित फैसलों पर जनता से सहयोग की अपील भी की है। यह फैसले क्या होंगे इसका अनुमान लगाना संभव नही होगा। लेकिन पिछले कुछ समय में आर्थिक मुहाने पर जो कुछ घट जाता है उस पर नजऱ दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। इन घटनाओं में दो प्रमुख घटनाएं पहले पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक और फिर यस बैंक पर आरबीआई के प्रतिबन्ध रहे हैं। पीएनबी का कार्य और प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित था। क्योंकि शायद उसके खाता धारकों की संख्या ही 50,000 के आप पास थी। इसलिये वह मुद्दा ज्यादा नही बढ़ां परन्तु यस बैंक से 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई राज्य सरकारों का पैसा उसमें जमा था। कई राज्यों के सहकारी बैंक उससे प्रभावित हुए हैं। यस बैंक के इस बड़े प्रभाव क्षेत्र के कारण आरबीआई को इसे बड़ा कर्ज देकर खाताधारकों के हितों रक्षा के लिये समाने आना पड़ा है।
लेकिन आरबीआई के पास भी रिजर्व धन इस देश के आम आदमी का हैं जबकि बैंक एनपीए के कारण फेल हो रहे हैं और यह एनपीए अंबानी जैसे बड़े उद्योग घरानों का है। इस बड़े कर्ज की वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये नही जा रहे हैं। यह एनपीए आज दस लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। इसलिये जब तक कर्ज वसूल नही हो जाता है तब तक बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंकों की हालत हाथ खड़े करने तक पहुंच चुकी है और आरबीआई हर बैंक को कर्ज देकर नही बचा पायेगा। इसी वस्तुस्थिति के कारण रेटिंग ऐजैन्सीयां हर बार विकास दर के अनुमान बदलने पर विवश हो रही हैं। सरकार को विनिवेश का आंकड़ा इस बार दो लाख करोड़ करना पड़ा है। आज कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति को और धक्का लगा है। पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो कदम कोरोना को रोकने के लिये उठाये जा रहे हैं उनका सीधा प्रभाव व्यापार और रोज़गार पड़ना शुरू हो गया है इससे प्रभावित हो रहे लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगना शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि यह स्थिति और कितने दिन तक ऐसे ही चलेगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिये सरकार एनपीए की वूसली के लिये कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर खाता धारकों से इस घाटे को पूरा करने के लिये कोई अंशदान मांगा जाता है इसका खुलासा तो तभी हो पायेगा जब टास्क फोर्स का कोई फैसला सामने आता है जिस पर जन सहयोग का आह्वान किया जायेगा। लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों मे ऐसा कुछ अवश्य देखने को मिलेगा। महामारी के परिप्रेक्ष में प्रधानमंत्री को हर तरह का जनसहयोग दिया जाना चाहिये। लेकिन इसमें आम आदमी के हितों की रक्षा करना भी प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी हो जाती है।
सिन्धिया कांग्रेस के लिये घातक होंगे या भाजपा के लिये अर्थहीन
- Details
- Created on Wednesday, 18 March 2020 11:02
- Written by Shail Samachar