


ShareThis for Joomla!
जब प्रधानमंत्री ही आक्रामक होने को कहे तो...
- Details
- Created on Tuesday, 04 February 2020 11:55
- Written by Shail Samachar
 नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उभरा नागरिक विरोध जामिया और शाहीन बाग में गोली चलने के बाद भी जारी है। इन दोनों जगह गोली चलाने वाले युवा स्कूल और कालिज जाने वाले छात्र हैं। जिन्होने शायद इस संशोधन को पढ़ भी नही रखा होगा समझ आना तो और भी दूर की बात होगी। इस संशोधन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सौ से अधिक याचिकायें दायर हैं। केन्द्र सरकार ने इन पर जवाब दायर करने के लिये एक माह का समय मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं में इसके हर पक्ष पर सवाल उठाये गये हैं। एनआरसी, एनपीआर और सीएए में क्या संबंध है इस पर सवाल है। इस पर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और अन्य मन्त्रियों एवम् नेताओं के संसद के भीतर दिये गये ब्यानों को भी अदालत के संज्ञान में लाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संशोधन पर उठे हर सवाल और हर शंका के समाधान का सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा और कोई मंच नही हो सकता। लेकिन इस मंच से कोई जवाब आने से पहले ही इसका विरोध कर रहे लोगों को गद्दार कहना, उन्हे टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थक बताना किसी भी अर्थ में जायज नही ठहराया जा सकता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उभरा नागरिक विरोध जामिया और शाहीन बाग में गोली चलने के बाद भी जारी है। इन दोनों जगह गोली चलाने वाले युवा स्कूल और कालिज जाने वाले छात्र हैं। जिन्होने शायद इस संशोधन को पढ़ भी नही रखा होगा समझ आना तो और भी दूर की बात होगी। इस संशोधन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सौ से अधिक याचिकायें दायर हैं। केन्द्र सरकार ने इन पर जवाब दायर करने के लिये एक माह का समय मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं में इसके हर पक्ष पर सवाल उठाये गये हैं। एनआरसी, एनपीआर और सीएए में क्या संबंध है इस पर सवाल है। इस पर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और अन्य मन्त्रियों एवम् नेताओं के संसद के भीतर दिये गये ब्यानों को भी अदालत के संज्ञान में लाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संशोधन पर उठे हर सवाल और हर शंका के समाधान का सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा और कोई मंच नही हो सकता। लेकिन इस मंच से कोई जवाब आने से पहले ही इसका विरोध कर रहे लोगों को गद्दार कहना, उन्हे टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थक बताना किसी भी अर्थ में जायज नही ठहराया जा सकता है।
शाहीन बाग में विरोध पर बैठे लोगों की मांग है कि सरकार उनकी बात सुने। कानून मन्त्री रवि शंकर प्रसाद ने जब यह ब्यान दिया कि सरकार इन लोगों से बात करने के लिये तैयार है लेकिन फिर उसी दिन प्रधानमन्त्री का ब्यान आ जाता है कि भाजपा को इस पर आक्रमकता से अपनी बात रखनी होगी। प्रधानमन्त्री का यह ब्यान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक निर्देश है। प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री ने जब विरोधियों पर आरोप लगाया कि यह लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई आरोप नही हो सकता। ऐसे लोग सही में राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं। जब देश का प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री इतना बड़ा आरोप लगाये तो स्वभाविक है कि यह आरोप तथ्यों पर आधारित होगा। क्योंकि तब किसी के खिलाफ इस निष्कर्ष पर पहंुचेंगे कि वह देश के टुकड़े-टुकड़े करने की बात कर रहा है तो तय है कि यहां तक पहुंचने से पहले देश की गुप्तचर ऐजैन्सीयों ने इस संद्धर्भ में सारे प्रमाण जुटा लिये होंगे। इसके लिये मानदण्ड तय कर लिये गये होंगे कि किस आधार पर किसी का ऐसा वर्गीकरण किया जायेगा। प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री के इन आरोप पर जब गृह मन्त्रालय से आरटीआई के माध्यम से यह सूचना मांगी गयी कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर सरकार के पास क्या जानकारी है। क्या इसके लिये कोई मानदण्ड बनाये गये हैं। क्या इसकी कोई सूची उपलब्ध है। इस तरह की सारी जानकारियां एक अंग्रेजी दैनिक एक्सप्रैस के पत्रकार ने मांगी थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस टुकड़े-टुकड़े गैंग को लेकर पूरी अनभिज्ञता जाहिर की। उसके गृह मन्त्रालय के पास कोई जानकारी ही नही है। अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। जिस पर किसी का कोई खण्डन नही आया है। इस तरह आरटीआई के जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह का संबोधन/आरोप बिना किसी प्रमाण के ही लगा दिया गया। आज हर छोटा-बड़ा नेता इस आरोप को हवा दे रहा है।
दिल्ली चुनावों के प्रचार में जब अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के ब्यानों का कड़ा संज्ञान लेते हुय चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबन्ध लगाया तो भाजपा ने इस प्रतिबन्ध का विरोध करते हुए चुनाव आयोग में इस पर आपति दर्ज करवाई। यह आपति दर्ज करवाने का अर्थ है कि भाजपा प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के ब्यानों का समर्थन करती है। आज जब प्रधानमन्त्री ने पार्टी को निर्देश दिया है कि वह आक्रामक होकर इस संशोधन पर अपना पक्ष रखें तो स्वभाविक है कि अनुराग और प्रवेश वर्मा की तर्ज के कई और ऐसे ही ब्यान देखने को मिलंेगे। जिस तरह से जामिया और शाहीन बाग में दो छात्रों ने गोली चलायी है ऐसे ही कई और छात्र देश के अन्य भागों में भी देखने को मिल जायें तो क्या उससे कोई हैरानी होगी क्योंकि इस मुद्दे पर तर्क तो सर्वोच्च न्यायालय में ही सामने आयेगा जहां सरकार और याचिकाकर्ता खुलकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। अभी इस संशोधन पर उभरा विरोध थमा नही है और इसी बीच शाहीन बाग में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा तैयार किये गये भारतीय संविधान को लेकर भी चर्चा उठ गयी है। यह आरोप लगाया गया है कि यह नया संविधान हिन्दु धर्म पर आधारित है। इसके मुताबिक भारत को एक हिन्दु राष्ट्र घोषित कर दिया जायेगा। इस कथित संविधान का संक्षिप्त प्रारूप सोशल मीडिया के मंच पर आ चुका है। लेकिन इस कथित संविधान को लेकर सरकार और संघ की ओर से कोई स्पष्टीकरण/खण्डन जारी नही किया गया है। यह संविधान पूरी तरह मनुस्मृति पर आधारित है। आज पूरे देश में ही नही बल्कि यूरोपीय यूनियन के मंच तक नागरकिता संशोधन अधिनियम चर्चा और विवाद का विषय बन चुका है। ऐसे में इसी समय इस सविंधान की चर्चा उठना और बड़े गंभीर संकेत और संदेश देता है जिस पर समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है।
हर विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं होता
- Details
- Created on Tuesday, 28 January 2020 12:06
- Written by Shail Samachar

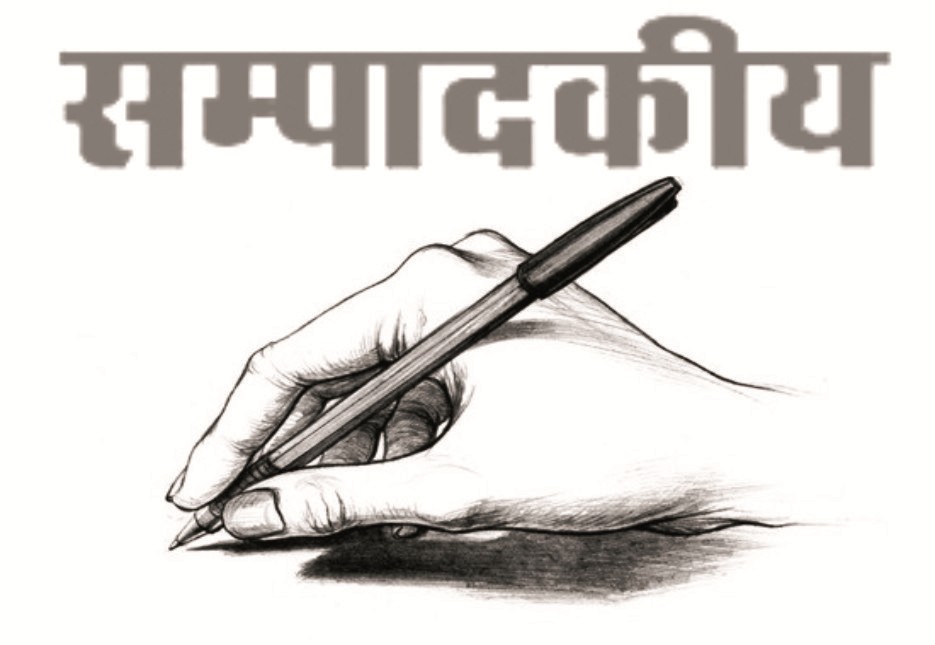
लेकिन क्या सही में इतनी सी ही बात है? नहीं यह सब कुछ इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह मसला असम में एनआरसी लागू होने से शुरू हुआ। असम में 1971 में पाकिस्तान विभाजन से बने बंग्लादेश से लाखों की संख्या में आये बंगलादेशी शरणार्थीयों से शुरू होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग वापिस बंगलादेश जाने की बजाये यहीं रह गये थे। इन लोगों के यहीं रह जाने से असम के मूल लोग प्रभावित हुए और इन लोगों को वापिस बंगलादेश भेजने के लिये असम के युवाओं और छात्रों ने बड़ा आन्दोलन किया। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इन आन्दोलनरत छात्रों के साथ समझौता किया कि 24 मार्च 1971 के बाद आये बंगलादेशीयों को वापिस भेजा जायेगा। असम गण परिषद की सरकार इसी आन्दोलन के परिणामस्वरूप बनी थी। इस समझौते को लागू करवाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका तक दायर हुई। इस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने असम में ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये। इन निर्देशों पर अमल करते हुए जो सूची तैयार की गयी उसमें करीब 20 लाख लोग गैर नागरिक पाये गये। असम में जब एनआरसी की यह प्रक्रिया चल रही थी तभी गृहमन्त्री ने संसद में यह कह दिया कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। असम मे जो बीस लाख लोग गैर नागरिकों की सूची में आये उनमें ज्यादा जनसंख्या हिन्दुओं की है। हिन्दुओं की संख्या ज्यादा होने और एनआरसी के विरोध के चलते असम के सवाल को यहीं पर खड़ा कर दिया गया है।
असम की समस्या का कोई हल निकालने के स्थान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम ला दिया गया और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बंगलादेश से आये गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया गया। इस नागरिकता के लिये आधार तैयार करने का काम एनपीआर से शुरू कर दिया गया। एनपीआर हर उस व्यक्ति की गणना करेगा जो किसी स्थान पर छः माह से रह रहा है या रहना चाह रहा है। यह जनसंख्या का रजिस्टर है नागरिकों का नहीं। इसमें हर व्यक्ति गिनती में आयेगा चाहे वह नागरिक है या नही। जो व्यक्ति यहां का नागरिक है उसे अपनी नागरिकता के प्रमाण में दस्तावेज देने होंगे। उसे अपने पैरेन्टस और ग्रैन्ड पैरेन्टस का प्रमाण देना होगा। इसमें गलत सूचना देने पर दण्ड का भी प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि कोई भी आपके ऊपर सन्देह जता सकता है। सन्देह जताने से आप सन्देहशील की सूची में आ जायेंगे। इस सूची में आने से ही समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। एनपीआर पर कारवाई शुरू हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के उन्नीस जिलों में एनपीआर में 49 लाख सन्देहशील श्रेणी में आ गये हैं। ममता बैनर्जी के अनुसार चैदह लाख दार्जलिंग में प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह यह माना जा रहा है कि एनपीआर के माध्यम से करोड़ों लोग सन्देहशील नागरिकों की श्रेणी में आ जायेंगे। अब देखना यह है कि इसमें किस समुदाय के कितने लोग आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है। एनपीआर में आने वाले लोग डाटा के आधार पर ही एनआरसी और नागरिकता संशोधन का काम आगे बढ़ेगा।
सरकार को संसद में मिले प्रचण्ड बहुमत के आधार पर अपने ऐजैण्डे को आगे बढ़ा रही और उसका ऐजैण्डा भारत को भी धर्म के आधार पर हिन्दु राष्ट्र बनाने का है यह हर रोज सार्वजनिक होता जा रहा है। धर्म की मादकता के आगे तर्क गौण हो चुका है। आज देश लोकतन्त्र के हर स्थापित मानक पर नीचे आता जा रहा है। विश्व समुदाय की नजर मे भारत की साख लगातार गिरती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय भी महत्वपूर्ण सवालों को लंबित रखने की नीति पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है लेकिन वहां के तीनों पूर्व मुख्यमन्त्री अभी तक नजऱबन्द चल रहे हैं। देश के मीडिया का सच कोबरा पोस्ट के स्टिंग आप्रेशन के माध्यम से सामने आ चुका है। जिसमें तीन दर्जन से अधिक बड़े मीडिया संस्थान कैसे बिकने को तैयार और किस हद तक विपक्ष के बडे नेताओं का सुनियोजित चरित्र हनन करने पर सहमत हो जाते हैं इससे देश की स्थिति का पता चल जाता है। आर्थिक तौर पर देश कितना कमजोर हो चुका है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार फिर आरबीआई से पैसे की मांग कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता संशोधन पर टकराव बढ़ा कर आर्थिक असफलता को लम्बे अरसे तक छुपाया जा सकेगा? शायद नही। हर विरोध को राष्ट्रद्रोह कहकर चुप नही कराया जा सकता। आज टुकड़े-टुकड़े गैंग के सवाल पर आरटीआई में सूचना के बाद प्रधानमन्त्री और गृहमंत्री का कद बहुत छोटा हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक नागरिकता संशेाधन वापिस लिया जाये
- Details
- Created on Tuesday, 21 January 2020 06:58
- Written by Shail Samachar

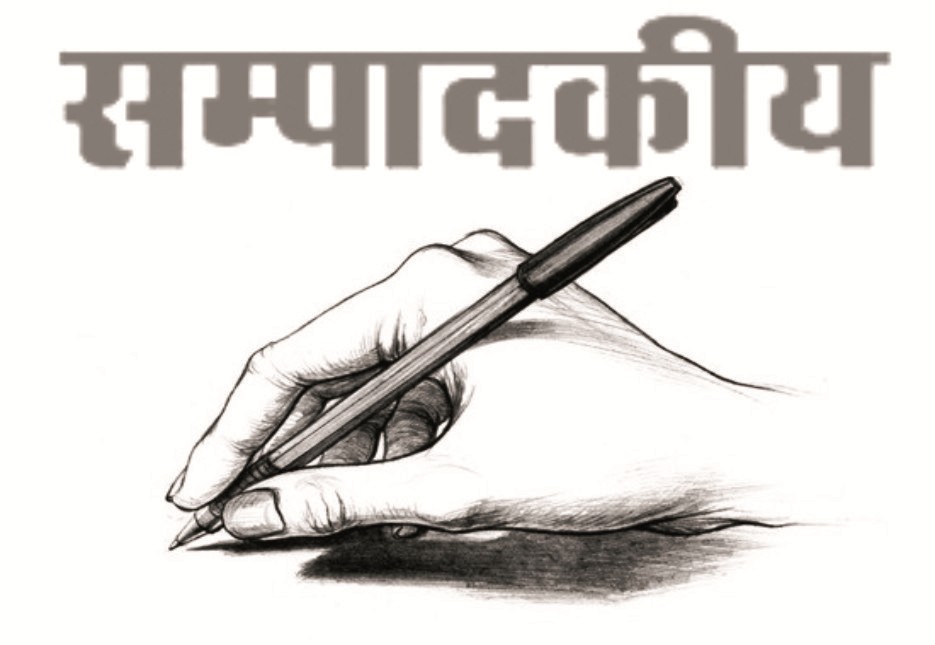
इस समय नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में आ चुकी हैं उससे पता चलता है कि देश में इसका विरोध कितना हो रहा है। शायद आज तक इतना विरोध किसी भी मुद्दे पर नही उभरा है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर का जिस भी व्यक्ति ने ईमानदारी से अध्ययन किया है वह मानेगा कि तीनों में गहरा संबंध है बल्कि एनपीआर ही सबकी बुनियाद है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अैर उनके मन्त्री इस विषय पर कुछ भी बोलते हैं तो उससे सरकार और नेतृत्व की नीयत पर ही सवाल खड़े होने लग जाते हैं। राज्य मन्त्री किरन रिजजू ने राज्य सभा में 24-7-2014 को एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं यह माना है कि एनपीआर ही इस सबका आधार है। स्थितियां जो 2014 में थी वही आज भी हैं। यह सही है कि अवैध घुसपैठिये और धर्म के कारण प्रताड़ित हो कर आने वाले व्यक्ति में फर्क होता है। प्रताड़ित की मद्द की जानी चाहिये घुसपैठिये की नहीं लेकिन फर्क कैसे किया जायेगा सवाल तो यह है। क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नही रखा गया है। जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं उससे यही संकेत उभरता है कि केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बाहर का रास्ता दिखाने की बिसात बिछायी जा रही है।
प्रधानमन्त्री कह चुके हैं कि एनआरसी को लेकर कहीं कोई चर्चा ही नही हुई है और जब इस पर सरकार में कोई चर्चा कोई फैसला ही नही हुआ है तब एनपीआर को लेकर कोई प्रक्रिया क्यों शुरू की जा रही है इसके लिये धन का प्रावधान क्यों किया जा रहा है। एनपीआर का प्रतिफल तो एनआरसी और सीएए में आयेगा। जब एनआरसी लागू ही नही किया जाना है तो एनपीआर का बखेड़ा ही क्यों शुरू किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं पर सरकार को यह जवाब देना है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी एक तरफ प्रधानमंत्री और उनके मन्त्रीयों के ब्यान होंगे और दूसरी एनआरसी, सीएए तथा एनपीआर पर जारी सरकारी आदेश होंगे। सबका मसौदा सामने होगा। यह स्थिति एक तरह से सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनो के लिये परीक्षा की घड़ी होगी। इस परीक्षा में दोनो का एक साथ पास होना संभव नही है। लेकिन किसी एक का भी असफल होना देश के लिये घातक होगा। आज देश की अर्थव्यवस्था भी एक संकट के दौर से गुजर रही है और इसे नोटों पर महात्मा गांधी की जगह लक्ष्मी माता की फोटो छापकर उबारा नही जा सकता जैसा कि भाजपा नेता डा. स्वामी ने सुझाव दिया है। इस समय सरकार को अपने ऐजैण्डे से हटकर नागरिकता संशोधन को वापिस सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्व सहमति से इसका हल निकालना होगा। यदि ऐसा नही हो पाता है तो आने वाला समय नेतृत्व को माफ नही कर पायेगा।
नागरिकता संशोधन पर कमजोर है सरकार का पक्ष
- Details
- Created on Monday, 13 January 2020 11:03
- Written by Shail Samachar


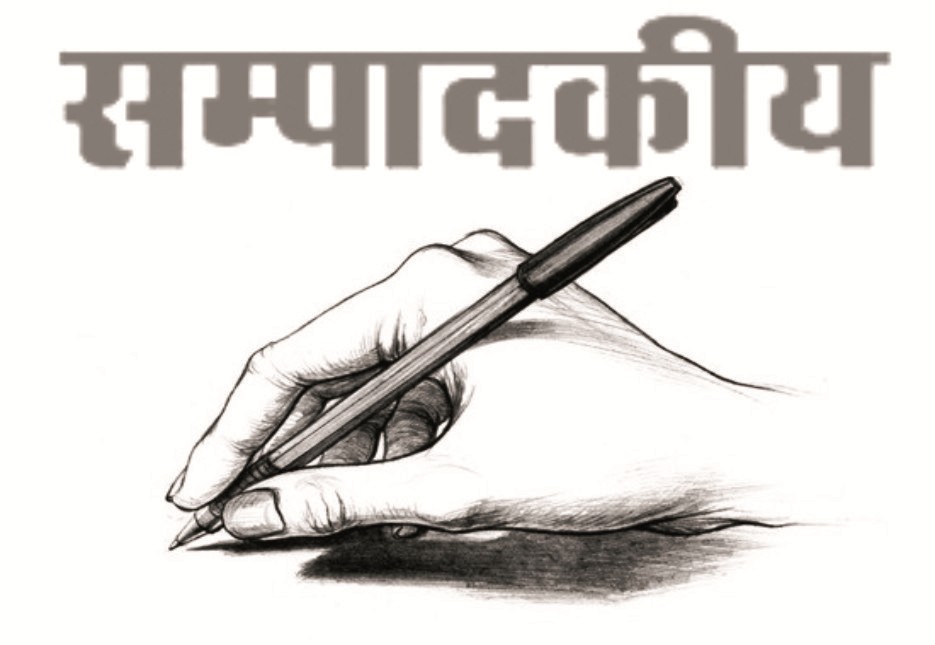
इस परिदृश्य में यदि सारी वस्तुस्थिति का आकलन किया जाये तो सबसे पहले यह सामने आता है कि सरकार इस संशोधन को लेकर यह तर्क दे रही है कि देश की जनता ने उसे इसके लिये अपना पूरा समर्थन दिया है क्योंकि उसने लोकसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्रा में इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। आज सत्ता में आने पर उसी घोषणा पत्रा को अमली शक्ल दी जा रही है। भाजपा का यह चुनाव घोषणा पत्र मतदान से कितने दिन पहले जारी हुआ था और इस पर कितनी सार्वजनिक बहस हो पायी थी यह सवाल हर पक्षधर को ईमानदारी से अपने आप से पूछना होगा। भाजपा को देश के कुल मतदाताओं के कितने प्रतिशत का समर्थन हासिल हुआ है यदि इसका गणित सामने रखा जाये तो बहुजन के समर्थन का दावा ज्यादा नही टिक पायेगा यह स्पष्ट है। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा और जेडीयू ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन आज नितिश कुमार ने कहा है कि वह इस विधयेक पर अपने राज्य में अमल नही करेंगें यही स्थिति शिवसेना की है। लोस चुनावों में भाजपा के साथ थी लेकिन आज अलग होकर अपनी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में इस विधयेक को लागू न करने की घोषणा की है। आकाली दल भी खुलकर इस अधिनियम के पक्ष में नही आया है। आखिर क्यों भाजपा के सहयोगी रहे यह दल नागरिकता संशोधन का समर्थन नही कर रहे हैं।
गैर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने इस अधिनियम पर अपने-अपने राज्यों में अमल करने से मना कर दिया है। जब से इस संशोधन को लेकर विवाद, खड़ा हुआ है उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को सीधे समर्थन नही मिला है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में सभी सीटें जीतने के बाद विधानसभा में अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नही कर पायी। झारखण्ड भी उसके हाथ से निकल गया है। इस समय देश के दस बड़े राज्यों के मुख्यमन्त्री खुलकर इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केन्द्र और राज्यों में किसी मुद्दे पर टकराव की स्थिति उभरी है। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पांच दर्जन याचिकाएं आ चुकी है। इसके अतिरिक्त कई उच्च न्यायालयों में भी ऐसी ही याचिकाएं आ चुकी हैं। केरल विधानसभा तो इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर तब तक सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है जब तक हिंसा थम नही जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का पिछले अरसे से संवदेनशील मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई न करने का रूख रहा है। कश्मीर मुद्दे पर लम्बे समय तक सुनवाई नही की गयी।ं जेएनयू हिंसा से लेकर छात्र हिंसा से जुडें सभी मुद्दों पर सुनवाई लंबित की गयी है। यदि इन मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से सुनावाई हो जाती तो बहुत संभव था कि हालात इस हद तक नही पहुंचते। क्योंकि दोनांे पक्ष अदालत के फैसले से बंध जाते परन्तु ऐसा हो नही सका है।
आज विश्वविद्यालयों का छात्र इस आन्दोलन में मुख्य भूमिका में आ चुका है क्योंकि वह इन मुद्दों के सभी पक्षों पर गहन विचार करने की क्षमता रखता है। विश्वविद्यालय के छात्र की तुलना हाई स्कूल के छात्र से करना एकदम गलत है। विश्वविद्यालय के छात्र में मुद्दों पर सवाल पूछने और उठाने की क्षमता है। उसे सवाल पूछने से टुकड़े-टुकड़े गैंग संबोधित करके नही रोका जा सकता है। आज प्लस टू का छात्र मतदाता बन चुका है। ऐसे में जब प्लसटू से लेकर विश्वविद्यालय तक का हर छात्र मतदाता हो चुका है और सभी राजनतिक दलों ने अपनी-अपनी छात्र ईकाईयां तक बना रखी है। हर सरकार बनाने में इस युवा छात्र की भूमिका अग्रणी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे पुराना छात्र संगठन है और संघ परिवार की एक महत्वपूर्ण ईकाई है। इस परिप्रेक्ष में आज के विद्रोही छात्र के सवालों को लम्बे समय तक अनुतरित रखना घातक होगा। किसी भी विचारधारा का प्रचार-प्रसार गैर वौद्धिक तरीके से कर पाना संभव नही होगा। किसी भी वैचारिक मतभेद को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा नही दी जा सकती है उसे आतंकी करार नही दिया जा सकता है। क्योंकि हर अपराध से निपटने के लिये कानून मे एक तय प्रक्रिया है उसका उल्लघंन शब्दों के माध्यम से करना कभी भी समाज के लिये हितकर नही हो सकता। नागरिकता संशोधन को इतने बड़े विरोध के बाद ताकत के बल पर लागू करना समाज के हित में नही हो सकता ।
सत्ता के दो वर्ष बाद
- Details
- Created on Sunday, 05 January 2020 11:51
- Written by Baldev Sharma

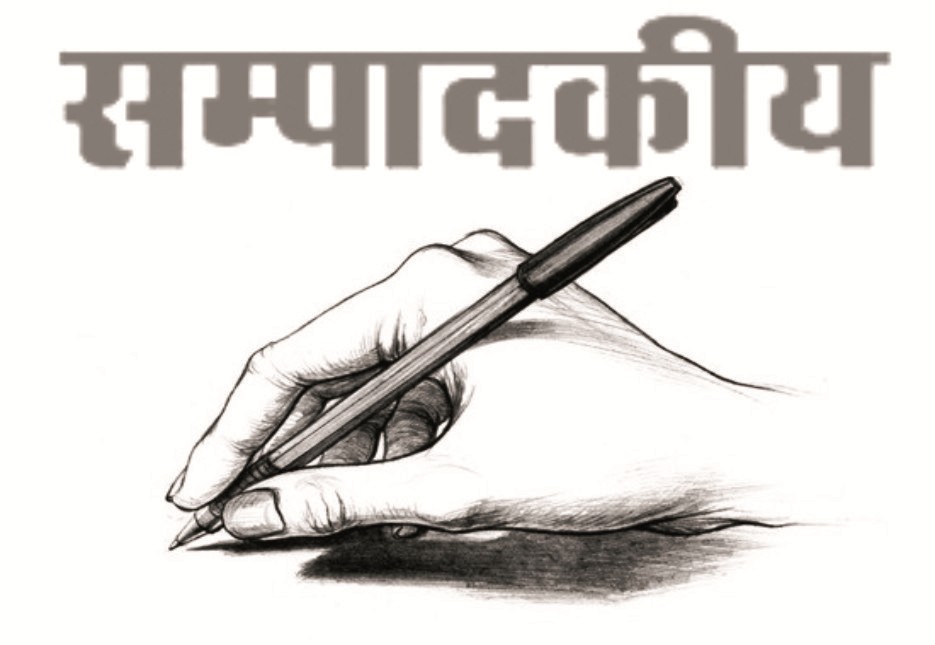
किसी भी सरकार के सत्ता के पहले दो वर्ष प्राईम टाईम माने जाते हैं। क्योंकि नीतिगत महत्वपूर्ण फैसले इसी शुरू के समय में लिये जाते हैं। अगले दो वर्षों में उन फैसलों पर अमल किया जाता है। अन्तिम वर्ष चुनाव का होता है और तब इस सब का परिणाम जनता के सामने स्वतः ही आ जाता है। इसलिये अक्सर दो वर्ष के बाद भी सरकारों को लेकर उनका सर्वे किये जाने का चलन भी आ चुका है। जयराम सरकार का भी एक ऐसा ही सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि यदि आज चुनाव हो जायें तो भाजपा को 25 से 27 सीटें ही मिल पायेंगी। इसी सर्वे के मुताबिक इन्वैस्टर मीट का असर केवल 14% जनता पर ही है। भाजपा के उच्च सूत्रों के मुताबिक यह सर्वे हाईकमान में भी चर्चित हुआ है। सूत्रों का दावा है कि जिस तरह की राष्ट्रीय परिस्थितियां आज बनती जा रही हैं उन्हें सामने रखते हुए इस तरह के सर्वे अन्य प्रदेशों को लेकर भी करवाये गये हैं। ‘‘आई विटनैस’’ के इस सर्वे का यदि प्रदेश की परिस्थितियों के संद्धर्भ में आकलन किया जाये तो यह सर्वे जमीनी हकीकत के बहुत नजदीक लगता है।
आज मीडिया और सरकारों में जिस तरह के संबंध बन चुके हैं और इन संबंधों के कारण सरकारों को जो श्रेष्ठता के प्रमाणपत्र मिल रहे हैं उनकी विश्वसनीयता भी उसी अनुपात में प्रश्नित हो चुकी है। पूर्व की धूमल और वीरभद्र सरकारों को थोक में यह श्रेष्ठता प्रमाण पत्र मिले हैं। यदि यह प्रमाण पत्र हकीकत के थोड़ा भी नजदीक होते तो यह सरकारें सत्ता में वापसी करती। लेकिन एक भी सरकार ऐसा नही कर पायी है। इससे सबसे ज्यादा मीडिया की अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठे हैं। इसलिये जयराम सरकार भी इस दिशा में कोई अपवाद सिद्ध नही हो पायेगी यह तय है। सरकार ने प्रदेश की जनता को इन दो वर्षों में क्या दिया है जिसका रिपोर्ट कार्ड लेकर यह सरकार जनता के सामने लेकर गयी है यदि उस पर निष्पक्षता से नजर डाली जाये तो स्थितियां बहुत निराशाजनक तस्वीर सामने रखती हैं। आम आदमी को रोजगार और मंहगाई सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि इन्ही के कारण उसकी रसोई, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट प्रभावित होता है। सरकार ने कितने लोगों को दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध करवाया है इसको लेकर विधानसभा के हर सत्र में सवाल आये हैं। इन सवालों के जवाब में कब क्या आंकड़े दिये गये है और कितनी बार यह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी को अगर इकठ्ठा रखकर कोई भी मंत्री या अधिकारी देखेगा तो शायद वह स्वयं ही शर्मसार महसूस करेगा क्योंकि यह सब कुछ सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित अधिकारिक सूचनाओं से मेल नही खाता है। शैल यह सारे दस्तावेजी प्रमाण अलग-अलग समय पर पाठकों के सामने रख चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सही हालत क्या है इसका खुलासा प्रदेश उच्च न्यायालयों में आयी याचिकाओं से लग जाता है जहां अदालत को संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के फरमान देने पड़े हैं। मंहगाई के प्रति सरकार की गंभीरता इसी से पता चल जाती है जब रसोई गैस और पैट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये गये तथा प्याज कम खाने की नसीहत दी गयी। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया उसमें इन मुद्दों का जिक्र तक नही किया गया।
विकास की स्थिति यह है कि प्रदेश के लिये केन्द्र द्वारा घोषित राष्ट्रीय राज मार्ग अभी तक सिद्धान्त रूप से आगे नही बढ़े हैं। प्रदेश की सड़कों और अन्य कार्यों के लिये केन्द्र से चैहद हजार करोड़ की मांग की गयी है। लेकिन अपने लिये दो सौ से ज्यादा गाड़ियां खरीद ली गयी। अपने वेतन भत्ते बढ़ा लिये गये और उस पर उठे जन रोष के बाद भी उसे वापिस नही लिया गया। सरकार के खर्चे चलाने के लिये हर माह कर्ज लिया जा रहा है। बजट से पहले और बजट के बाद टैक्स लगाये जाते रहे हैं लेकिन बजट को टैक्स फ्री घोषित/प्रचारित किया जाता है। जब सार्वजनिक जीवन में इतनी भी सुचिता नही रह जायेगी कि हम अपनी जनता से स्पष्ट ब्यानी कर सकें तो फिर ऐसे आयोजनों से क्या लाभ मिलेगा। इसीलिये इन आयोजनों को कर्ज लेकर घी पीने की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे में जब सरकार बजट के लिये सुझाव आमन्त्रित करने की बात करती है तब यही लगता है कि सरकार कैसे जनता को ना समझ मानकर चलती है। पिछले कई वर्षों से हर बजट टैक्स फ्री बजट दिया जाता रहा है और इसके बावजूद वस्तुओं और सेवाओं के दाम तथा सरकार की आय बढ़ती रही है। जयराम सरकार ने भी बजट के लिये सुझाव मांगे है ऐसे में सरकार से आग्रह है कि आप तो टैक्स फ्री बजट का झूठ अब जनता को न परोसने का साहस दिखायें। इसी के साथ यह सच्च भी स्वीकारें की बजट में दिखायी गयी पूंजीगत प्राप्तियां शुद्ध ऋण होती हैं और इस ऋण के साथ सरकार के कर्ज का आंकड़ा जनता के सामने रखने का साहस करें।



